Solved Question Answers, सूरदास
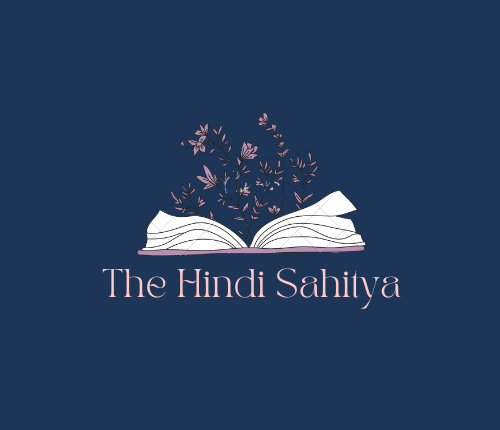
प्रश्न-2 सूरदास की काव्य कौशल का परिपाक भ्रमरगीत में किस प्रकार हुआ है? विश्लेषण कीजिए।
अथवा
सूरदास के काव्य कला पर विचार कीजिए।
उत्तर– सूरदास सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। वे पहले भक्त है और बाद में कवि है। सूरदास का काव्य अनेक भावात्मक और कलात्मक विशेषताओं से युक्त है।
अष्टछाप के कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। पुष्टिमार्गी होने के कारण सूर की भक्ति प्रेमाभक्ति थी। इसमें समर्पण को ही सब कुछ माना गया है।
सूरदास जी ब्रजभाषा में कविता रचने वाले पहले प्रमुख कवि है। उन्होंने ब्रज प्रदेश को लोक संस्कृति और वाचिक परम्परा की उत्कृष्टता प्रदान की है और कलात्मक उत्कर्ष प्रदान किया है। ब्रजभाषा में कृष्ण भक्ति से संबंधित भक्तिगीत की कीर्तन परम्परा में महत्त्वपूर्ण योगदान था।
ऐसा माना जाता है कि सूरदास जन्मांध थे, परन्तु कृष्ण लीलाओं और प्रकृति वर्णन की सजीवता उनके जन्मांध होने पर प्रश्नचिन्ह लगाती है। ‘सूरसागर’ नामक रचना इनकी कीर्ति का आधार है। इनके द्वारा रची अन्य रचनाओं में ‘सूरसारावली’ और ‘साहित्य लहरी’ प्रमुख है। ‘सूरसागर’ का भ्रमरगीत प्रसंग उल्लेखनीय है।
प्रकृति का साहित्य से गहरा संबंध है, जो कवि भावनाओं को अधिक महत्त्व देते हैं, उनके काव्य में प्रकृति का केन्द्रीय स्थान होना स्वाभाविक है। सूरदास ने भी अपने काव्य साहित्य में प्रकृति को महत्त्व दिया है। प्रकृति के साथ जितना गहरा लगाव और तन्मयता का संबंध सूर-काव्य में दृष्टिगोचर होता है, उतना कहीं नहीं।
सूरदास प्रेम के कवि है। सूरदास का मूल आधार शृंगार और वात्सल्य है। उन्होंने कृष्ण की चंचल क्रीडाओं और युवा कृष्ण के शृंगार के सजीले चित्रों की एक पूरी प्रदर्शनी ही संजो दी है। सूरदास जी के काव्य की विशेषताओं को निम्न बिन्दुओं के आधार पर समझ सकते हैं-
1. शृंगार-वर्णन- सूरदास ने ‘सूरसागर’ में राधा-कृष्ण और गोपियों के अनेक संयोगकालीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। सूरदास ने राधा-कृष्ण के प्रारम्भिक परिचय का आकर्षक वर्णन किया है। संयोग के साथ वियोग के भी अनेक चित्र मिलते हैं। कृष्ण मथुरा चले जाते हैं। गोपियाँ, राधा, यशोदा, गोप एवं ब्रज के सभी जड़-चेतन पशु-पक्षी उनके विरह से व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि संयोगकालीन सभी सुखप्रद वस्तुएँ गोपियों को कष्ट देले वाली हो जाती है। वे कहती हैं-
“बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै।”
तब वे लता लागति अति सीतल
अब भई विषम ज्वाला का पुंज।।
सूरदास का शृंगार वर्णन बहुत ही अद्भुत है। सूरदास का वियोग वर्णन बहुत ही सराहनीय है। उनके काव्य की महत्त्वपूर्ण विशेषता है।
2. वात्सल्य चित्रण- सूरदास प्रेम के कवि है। सूरकाव्य का मूल आधार शृंगार और वात्सल्य है। सूरदास वात्सल्य क्षेत्र के सम्राट है। उनके बाल-चित्रण में छोटी से छोटी बात भी नहीं छूटी है। उन्होंने कृष्ण के बाल सुलभ चेष्टाओं का सूक्ष्मातिसूक्ष्म निरीक्षण किया है। शृंगार वर्णन के साथ-साथ उनका वात्सल्य वर्णन भी सांगोपांग है। वर्णन की स्वाभाविकता उनके वात्सल्य पक्ष की विशेषताऐं हैं।
बाल चेष्टाओं के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भण्डार और कहीं नहीं है जितना सूरसागर में है। उदाहरण-
“सोभित कर नवनीत लिए।
घुटरूनि चलत रेनु तन मंडित, मुख दधि लेप किये।”
“मैया कबहि बढ़ैगी चोटी?
किसी बार मोहिं दूध पियत भई, यह अजहूँ है छोटी।”
3. दार्शनिक- सूरदास के दार्शनिक विचार वल्लभ सम्प्रदाय के सिद्धान्तों से प्रभावित है। निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन न करते हुए, उन्होंने सगुण भक्ति का प्रतिपादन किया। क्योंकि निर्गुण ब्रह्म का कोई रूप, गुण और जाति नहीं है, अतः चंचल मन बिना किसी आधार के इधर-उधर भटकता रहता है।
4. सूरदास का प्रकृति वर्णन- प्रकृति के साथ जितना गहरा संबंध और तन्मयता का संबंध सूर काव्य में दृष्टिगोचर होता है, उतना कहीं नहीं। हिन्दी के कवियों की तरह आमतौर पर सूरदास भी प्रकृति को उद्दीपन विभाव की तरह उपयोग किया है। प्रकृति मानो एक रंगमंच है जो नायक और नायिका की भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए विशेष वातावरण तैयार करती है, उदाहरण के लिए जो मधुवन संयोग के समय गोपियों को अतिप्रिय और शीतल लगता था वही कृष्ण के वियोग में दग्ध कर देने (जला देने) वाला प्रतीत होता है।
“बिन गोपाल बैरिन भई कुंजै।
तब ये लता लगति अति सीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजै।”
यह बात सही है कि सूरदास के प्रकृति वर्णन में वैविध्य कम है। चूँकि उनकी कविता में प्रकृति का भौगोलिक विस्तार कम है, इसलिए प्रकृति के सीमित रूप ही व्यक्त हुआ है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा है- “बाह्य प्रकृति के संबंध में सूरदास जी कि दृष्टि बहुत परिमित थी। एक तो ब्रज की गोचरणभूमि के बाहर उन्होंने पैर ही नहीं निकाला, दूसरा उस भूमि का भी पूर्ण चित्र उन्होंने कहीं नहीं खींचा।
5. सूरदास की भाषा- हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हुए सूरदास की भाषा किसी भी अध्येता को विस्मत में डाल देती है। सूरदास ने काव्य-भाषा के तौर पर ब्रजभाषा का प्रवर्तन तो किया ही, साथ ही इसे पूर्णता के ऐसे स्तर प्रतिष्ठित भी कर दिया जिसके लिए काव्यभाषा को एक लम्बी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है।
सूरदास की भाषा ब्रजभाषा होकर भी बोलचाल की भाषा नहीं है। वह सुनने में इतनी सहज और सरल है कि उसके लोकभाषा होने का आभास होता है। किन्तु, वास्तव में वह ब्रजभाषा का व्याकरणिक आधार लिए हुए कुछ अन्य भाषाओं के समन्वय से बनी भाषा है। उदाहरण के लिए उसमें ‘जेहि’ ‘तेहि’ जैसे अवधी प्रयोग हैं। इसी प्रकार पूर्वी के शब्दों, अवहट्ठ व पुरानी हिन्दी के भाषिक प्रयोग भी यदा-कदा दिख जाते हैं।
सूरदास की भाषा की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यन्त स्वाभाविकता के साथ किया गया है। जिसने इस भाषा में अद्भुत लोक प्रभाव व मार्मिकता का समावेश कर दिया है। उदाहरण-
“नन्द ब्रज लीजै ठोकि बजाई”
6. सूरदास की अलंकार योजना- सूरदास का काव्यात्मक सौन्दर्य बहुत हद तक अलंकारों पर आधारित है। अलंकार कविता के शोभाकारक धर्म माने गये हैं। जब ये काव्य के आन्तरिक गुणों के अनुरूप होते हैं तो कविता के सौंदर्य में अत्यन्त वृद्धि करते हैं किन्तु एक सीमा के बाद जब इनकी अति होने लगती है तो कविता का प्रभाव और सौंदर्य कमजोर होने लगता है। सूरदास की अलंकार योजना बहुलांश में उनकी कविता को प्रभावित/प्रभावशाली बनाती है किन्तु कहीं-कहीं ऐसे प्रसंग भी आये है जहाँ आचार्य शुक्ल के शब्दों में- “सूर को उपमा देने की झक सी चढ़ जाती है और वे उपमा पर उपमा, उत्प्रेक्षा पर उत्प्रेक्षा कहते चले जाते हैं।” दोनों पक्षों का गम्भीर विश्लेषण करते हुए सूरदास की अलंकार योजना का मूल्यांकन किया जा सकता है। सूरदास की कविता मूलतः भावनाओं की तीव्रता और सहृदयता की कविता है, इसलिए इसमें शब्दालंकारों का प्रयोग कम हुआ है।
7. सूरदास की बिंब योजना- हिन्दी साहित्य में यूँ तो बिंबों का प्रयोग लगभग हर कवि ने किया है किन्तु जो कवि अपनी बिंब क्षमता के लिए जाने जाते हैं उनमें सूरदास अव्वल है। यदि बिंब निर्माण क्षमता की दृष्टि से कोई उनसे मुकाबला कर सकता।
