Solved Question Answers, रामचंद्रिका: केशवदास
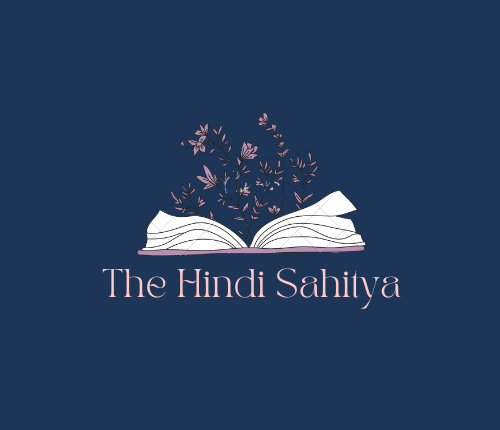
प्रश्न-2: केशवदास द्वारा रचित ‘रामचंद्रिका’ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
उत्तर- ‘रामचंद्रिका’ केशवदास द्वारा लिखित परंपरा का महाकाव्य है। जिसका रचनाकाल 1601 ई. है। इसमें रामकथा का वर्णन किया गया है एवं रामकथा के प्रमुख प्रसंगों को चुनकर और उन्हें विभिन्न छन्दों में क्रम देकर छंदबद्ध कर दिया गया है। इसमें अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें कवि में अपने सहृदयता को प्रमाणिक करने की कोशिश की है। केशव ने इसमें परंपरागत कथा को आधार बनाया है और रीति-युगीन दरबारी वैभव की युगीन परिस्थितियों में उसे अपने विचारों और भावों के अनुसार एक नवीन एवं मौलिक रूप प्रदान किया है।
‘रामचंद्रिका’ 39 प्रकाशों में विभक्त है। आरम्भ के 26 प्रकाशों में रामतिथक की कथा आती है। 27 से 32वें प्रकाश तक राजा-राम अनेक शासन तथा रामराज्य का चित्रण है। 33वें प्रकाश से अंतिम प्र प्रकाश तक सीता निर्वासन की कथा चर्चित है। इसमें केशवदास अपने भाव और विचार के अनुसार प्रसंगों का क्रमबद्ध वर्णन किया है। रामचंद्रिका की विशेषताएँ-
कथानक योजना- रामचंद्रिका में कुछ प्रसंग असाधारण रूप से समृद्ध और सशक्त है पर कुछ शिथिल और कमजोर हैं। कथानक के निर्माण में वाल्मीकि आदि प्रसिद्ध कवियों की रामकथा तथा भागवत आदि पुराणों के अतिरिक्त केशवदास में संस्कृत के साहित्य ग्रंथों से भी पर्याप्त सहायता ली है जिनमें ‘हनुमानटक’ एवं ‘प्रसन्नराघव’ प्रमुख है। संवादों की नाटकियता तथा और उक्ति वैचित्र्य पर इन ग्रंथों का विशेष प्रभाव पड़ा है। केशवदास ने ‘रामचंद्रिका’ का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कहा भी है- ‘रामचन्द्र की चन्द्रिका बरनत है। बहु दंद।’
संवाद योजना- ‘रामचंद्रिका’ केशवदास दूसरा ‘संवाद शैली’ में लिखित महाकाव्य है। ‘रामचंद्रिका’ की विशिष्टता उसकी संवाद योजना है। इनके जैसा संवाद कोई प्राचरन कवि नहीं लिख सका है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है- “रामचंद्रिका में केशवदास को सबसे अधिक सफलता मिली है। संवादों में उनका रावण-अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कही अधिक उपयुक्त एवं सुन्दर है। उदाहरण के लिए निम्नलिखित पंक्ति में संवादों की तीव्रता और चुस्ती द्रष्टव्य है क्योंकि एक ही कथन में चार संवाद दिये गऐ हैं-
“मातु कहाँ नृपतात? गए सुश्लोकहि। क्यों? सुत शोक लये।”
‘रामचंद्रिका’ में जो महत्त्वपूर्ण संवाद है वे है दशरथ-विश्वामित्र संवाद, सुमति विमति संवाद, रावण बाणासुर संवाद, जनक-विश्वामित्र संवाद, परशुराम-वामदेव संवाद, परशवुराम-राम संवाद, कैकेयी-भरत संवाद, शूर्पणखा-लक्ष्मण संवाद, रामजानकी संवाद, राम-लक्ष्मण संवाद, रावण-अंगद संवाद, सीता-रावण संवाद, सीता-हनुमान संवाद, रावण-हनुमान संवाद, लव-कुश-हनुमान संवाद आदि।
छंद योजना- ‘रामचंद्रिका’ में केशवदास की छंद योजना भी विशिष्ट है। उनकी बहुछंद की कल्पना नई वस्तु है। छंदों के सम्बंध में केशवदास छंदशास्त्र के प्रकांड पंडित ही नहीं उसके सफल प्रयोक्ता भी है। महाकाव्य और प्रबंध काव्य के अन्य रूपों में संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में केशव ने जैसी छंद योजना की है, वह किसी को प्राप्त नहीं होती।
जीवन दृष्टि- ‘रामचंद्रिका’ में केशवदास ने रामकथा को नए तरीके से प्रस्तुत किया। इसकी कथा संघर्ष की नहीं है। न तो वह सिर्फ भक्ति की रचना है। उसमें मौलिक तरीका अपनाते हुए भक्ति और राजवैभव दोनों पक्षों पर समान बल दिया गया है। कवि ने इसमें जो जीवन दृष्टि अपनायी है उसमें लौकिक और परलौकिक का अलगाव या विरोध लक्षित नहीं होता। केवल अंत में ज्ञान त्याग और भक्तों की वरीयता अवश्य सिद्ध होती है जो भारतीय संस्कृति की केन्द्रिय विशेषता रही है।
आलोचना के बिंदु- ‘रामचंद्रिका’ में केशवदास ने उचित संबंध निर्वाह नहीं किया है। इसमें मार्मिक प्रसंगों का ध्यान ठीक से नहीं रखा गया। जैसे एक छंद में राम का राज्याभिषेक, दूसरे छंद में राम को वनवास व भरत को राज देने का वरदान माँगना चित्रित कर दिया है। शुक्ल जी कहते हैं कि केशव में संबंध निर्वाह की क्षमता नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा है कि राम की कथा के भीतर जो मार्मिक स्थल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया है। तुलसीदास ने रामवनगमन प्रसंग को इतना मार्मिक व जीवंत बना दिया था जबकि केशवदास के वह एक सूचना मात्र रह गया। हालाँकि रामचंद्रिका में बहुछंदों की कल्पना नई वस्तु है किन्तु शुक्ल जी ने इसकी आलोचना करते हुए इसे छंदों का ‘अजायबघर’ कहा है उनका दावा है कि ‘रामचंद्रिका’ में छंद प्रयोग भाषा में प्रवाह एवं जीवंतता उत्पन्न नहीं करता।
निष्कर्ष- केशवदास को रामचंद्रिका के संवाद योजना, कथानक योजना में अद्वितीय सफलता प्राप्त हुई है। इनके जैसा संवाद दुर्लभ है किंतु छंद योजना एवं कथा को मार्मिक प्रसंगों को केवल सूचना मात्र के रूप में प्रस्तुत करने के कारण ‘रामचंद्रिका’ रामचरितमानस की तरह लोक ग्राही न हो सका।
