Solved Question Answers, घनानन्द
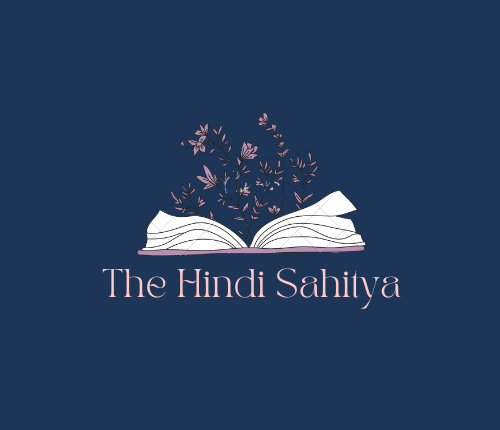
प्रश्न-1: घनानंद प्रेम की पीर के कवि है, इस कथन के आधार पर घनानन्द का काव्य सौंदर्य स्थापित कीजिए।
उत्तर– घनानंद रीतिकाल के सर्वाधिक मार्मिक कवियों में से है। वे प्रेमानिरूपण के ही केवल कवि नहीं है। वरन् वे स्वयं नेही महा है। प्रेम ही उनके काव्य का प्राण तत्व है। इनको विरहानुभूति गीति-कवियों की भांति नही है। वह अन्दर ही अन्दर ……. है। कवि की प्रेमानुभूति विश्छलता के साथ लौकिकता स्वाभाविकता, संयोगशीलता, कष्टसहिष्णुता और विरहातुरता से अनुप्राणित है। रीतिकाल के अन्य कवियों की अपेक्षा स्पष्टतया ही भिन्न एवं महत्त्वपूर्ण है। ‘ब्रजनाय’ ने उनके लिए नेही महा ब्रजभाषा ‘प्रवीन’ शब्दों का प्रयोग किया है और घनानंद की कविता को समझने वाले के लिए ‘हिय-आंखिन नेह की पीर तकी’ का अनुबन्ध लगाया है। ‘स्वच्छन्द मार्ग सर्वाधिक भाव की स्वच्छन्दता का ही परिणाम है। उन्होंने प्रेम के मार्ग को अतिसूधा कहा है जो इस बात का अभिव्यंजक है कि प्रेमाभिव्यक्ति नायक और नायिका के माध्यम से नहीं अपितु इस स्वमेव स्वाभिव्यक्त है।
घनानंद ने प्रेम का सैद्धान्तिक विश्लेषण तो किया ही है साथ ही सुजान के प्रति अपनी भावना की अभिव्यक्ति के द्वारा उसका व्यावहारिक रूप भी स्पष्ट कर दिया है। सुजान के विषय में ऐतिहासिक तथ्याचार, जनश्रुतियों से ही संचित किये गये हैं किन्तु उनमें किसी प्रकार की मिथ्या सम्भावना निश्चित ही नहीं है। घनानंद गायक थे, कवि थे, उत्कृष्ट प्रेमी थे और रीति की विलासिता में पंगे हुए रसिक व्यक्ति थे। उन्हें हिन्दी की और इस देश की लौकिक तथा अलौकिक प्रेम भावनाओं का पूर्ण परिचय था। उनके भक्ति भाव के पद अलौकिक प्रेम के प्रति उनके आग्रह के परिचायक है। श्रीकृष्ण को सुजान के ब्याज से संबोध्ाित करना श्लेष के आधार पर अर्थ चमत्कार भी है और हिन्दी काव्य में उनसे पूर्व वर्णित प्रेम का सभी रूपों में ग्रहण भी है। घनानंद उर्दू-फारसी की प्रेम-परम्परा से भी भली प्रकार परिचित थे। उनकी रचनाओं में ‘इश्कलता’ और ‘योगबेलि’ इसका प्रमाण है। अतः यह कहा जा सकता है कि इस कवि ने प्रेम को सभी रूपों में अनुभव किया है। ‘सुजान’ के प्रति आकांक्षा और श्रासक्ति, तत्पश्यचात प्रेम जीवन में विश्वासघात के परिणामस्वरूप उत्पन्न कुण्ठा, निराशा और तड़प तथा प्रेम का उदात्तीकरण सभी घनांनद में विद्यमान है।
घनानंद की रचना में प्रेम के प्रति एक निश्चित और व्यवस्थित दृष्टिकोण उपलब्ध होता है। उन्होंने अपनी अनुभूति के बल पर प्रेम-तत्त्व को पहचान लिया है। प्रेम के विषय में उनकी सर्वप्रधान मान्यता है-
“अति सूधो सनेह को मारग है,
जहाँ नेकु सयानप बांक नहीं। तहाँ सांचे चले तजि आपुनपौ,
इझके कपटी जे निसाकं नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो
यहाँ एक ते दूसरो आँक नहीं।”
अर्थात्-
- प्रेम का मार्ग सरल-सहज है।
- उसमें कपट, अविश्वास और विश्वासघात का कोई स्थान नहीं।
- उसके लिए अपनेपन कोय स्व कोय अहंकार को छोड़ना पड़ता है।
घनानंद कहते हैं कि जो प्रेम करता है उसका मन अत्याधिक उछाले भरता है। हृदय में सौ-सौ भाव उमड़ते हैं, कामनाएँ सतरंगी हो उठती हैं। घनानंद की कविता में अभिलााषाओं का बड़ा विस्तृत और मार्मिक चित्रण है। उनका एक-एक अंग जैसे अनेक प्रकार की भाव-क्षुधा से मुक्त हो उठा है। वे सुजान को अनेक प्रकार से देखना चाहते हैं, उस पर रीझ जाना चाहते हैं। अंतर की भावाभिव्यक्ति सुजान को देखते ही जैसे पर लगा कर उड़ने लगती है। वे उस अभिव्यक्ति को, प्रेम की आग को संभाल नहीं पाते, अभिलाषा उन्हें हंसाती, रूलाती है-
“प्रेम आग जागै लागै उभर घन आनन्द को,
रोइबो न आबै तो पै गाइबो हू रोइबो।”
घनानंद का प्रेम प्रथम दर्शन जन्य ही है। उन्होंने सुजान की छवि को जब से देखा तभी से वे अनुरक्त हो गए-
“जब ते निहारे घन आनन्द सुजान प्यारे,
तब ते अनोखी आगी लागि रही चाह की।”
घनानंद ने प्रथम दर्शन के संकेत कई स्थलों पर दिए हैं और अपनी तज्जन्य व्याकुलता का अनेक प्रकार से चित्रण किया है। उनके नेत्रों के पैर प्रिय के पीछे-पीछे जाने लगे-
“जहाँ तँ पधारे मेरे नैनन ही पांव थारे,
बारे पे विचारे प्रारण पैंड-पैंड पे मनो।”
प्रेम की अनोखी रीति है कि यह एक सूक्ष्म दर्शनबिन्दु से बढ़कर जीवन को व्याप्त कर लेती है। घनानंद के काव्य में प्रथम दर्शन-जन्य प्रेम की व्याकुलता ही आगे चलकर जीवन के अगम्य विस्तार में फैल जाती है।
प्रेम की व्यथा, उसकी पीड़ा मधुर है। व्यथा उसे मिठास, माधुर्य के आधिक्य से बचाती है। आवश्यकता से अधिक मधुर भी स्वाद के लिए अरुचिकर हो जाता है। इस प्रकार व्यथा प्रेम के संयोग पक्ष के लिए अंकुश के समान है। स्वच्छन्द कवियों ने अपने अन्दर की आरति का, अपने हृदय की दयालुता का बड़ा मार्मिक चित्रण किया है। ‘घनानंद’ ने स्पष्ट कहा है-
“यह कैसा संजोग न बूझ परै,
जो वियोग न क्यूँ हूँ विछोहत है।”
सामान्यतयाः प्रिय के वियोग की स्थिति में व्यथा का महत्त्व और भी बढ़ जाता है। तब वह प्रेम जीवन का अंग हो जाता है।
घनानंद ऐसे चातक हैं जो सुजान रूपी घन के जल के नित्य प्यासे हैं। घनानंद में अधिकतर अशरीरी प्रेम के ही दर्शन होते हैं और उपभोग के स्थान पर प्रिय शृंगार के प्रति एक अभिलाषा और आसक्तिमयी आस्था ही दिखाई पड़ती है। घनानंद ने अपनी अनुभूति का अधिकार उदात्तीकरण कर लिया है। जिसमें प्रेम को जीवन-व्यापार के रूप में ही अपना लिया हो या जो प्रिय पर ही सर्वस्व वार देने का प्रण लेकर बैठा हो तो उसके लिए प्रेम काव्यगत आवश्यकता ही नहीं, एक अनिवार्यता भी है।
आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी घनानंद के प्रेम वर्णन के वैशिष्ट्य को निरूपित करते हुए कहते हैं कि प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेममार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जबांदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ।
घनानंद मूलतः वियोग के कवि है। उन्होंने अपने साहित्य में बिहारी आदि की तरह संयोग व मिलन के चित्र नहीं खीचे हैं बल्कि प्रेम की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। शुक्ल लिखते हैं कि- “ये वियोग शृंगार के प्रधान मुक्तक कवि है।”
इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि इनका साहित्य स्वानुभूति का साहित्य है न कि सहानुभूति का। अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में कविताएँ रचने वाले घनानंद के बारे में दिनकर जी लिखते हैं कि- “दूसरों के लिए किराए पर आँसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में रो रहा है।” ‘प्रेम की पीर’ का कवि कहलाने के पक्ष में एक तर्क यह भी है कि इनका प्रेम वर्णन वैधानिकता, अति भावुकता व अपने साथी के प्रति एकनिष्ठता से युक्त है-
“अति सूधो सनेह को मारग है
जहाँ नेकु सयानक बाँक नहीं।”
घनानंद के यहाँ विरह की पीड़ा इतनी तीव्र है कि प्रतीक रूप में उनके साहित्य में सर्वत्र दिखाई देती है। सुजान के प्रति जो लौकिक प्रेम था, बाद में वही कृष्ण-राधा के प्रति अलौकिक स्तर पर व्यक्त होने लगा। पीड़ा इतनी गहरी है कि राधा-कृष्ण भक्ति के प्रसंग में भी सुजान के विरह को व्यक्त करते रहे-
“ऐसी रूप अगाधे राधे, राधे, राधे, राधे,
तेरी मिलिवे को ब्रजमोहन, बहुत जतन है साधे।”
इस प्रकार विरह की गहरी अनुभूति, वैयक्तिकता, एकनिष्ठता, तीव्र भावुकता व स्वानुभूति जैसे तत्त्व घनानंद को ‘प्रेम की पीर’ के कवि के रूप में स्थापित करते हैं।
