Solved Question Answers, केशवदास: रामचंद्रिका
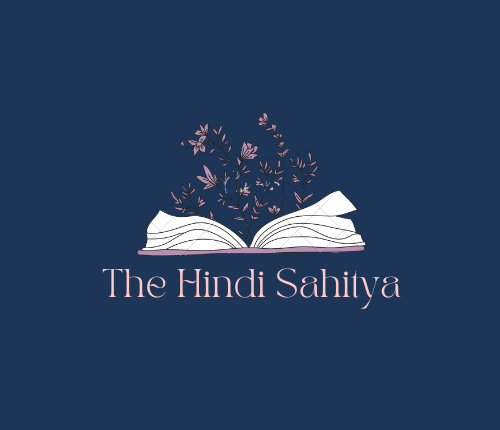
प्रश्न-1: ‘केशव कठिन काव्य के प्रीत है’- टिप्पणी कीजिए।
उत्तर– केशवदास जी को हिन्दी साहित्य का प्रमुख आचार्य और रसिक कवि माना जाता है। ये एक निर्भीक एवं स्पष्टवादी कवि थे। और यह इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी। ये एक रीतिकाल के प्रवर्तक कवि भी थे। उनकी समस्त रचनाऐं शास्त्रीय रीतिबद्ध हैं।
केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचन्द्र शुक्ल जी ने कहा है। केशवदास जी लक्षण ग्रंथों के लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे। हिंदी विषय में सर्वप्रथम केशवदास जी ने ही काव्य के विभिन्न अंगों का शास्त्रीय पद्धति से विवेचन किया था।
केशवदास अलंकारवादी कवि है। अतः चमत्कार प्रदर्शन के कारण उनके काव्य में कलापक्ष अधिक मुखर दिखाई पड़ता है। हृदय पक्ष का प्रायः अभाव ही लक्षित होता है और न्यूनाधिक है भी तो उस पर अलंकारों का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है।
इस प्रकार केशव को कठिन काव्य का प्रेम कहने के पीछे उनके काव्य में संस्कृत शब्दों की बहुलता है जो कि उनके संस्कृतमय पारिवारिक जीवन के कारण दरबारी कवि होने के कारण चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति अथवा आचार्यत्व था यही कारण है कि उनके विषय में यह उक्ति प्रचलित हो गयी है कि-
“कवि कौ देन च चहै विदाई। पूछे केशव की कविताई।।”
अतः केशव कठिन काव्य के प्रेत है का मूल्यांकन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत करना समीचीन होगा-
- क्लिष्ट कल्पनायुक्त वर्णन
- स्वाभाविक विरह वेदना से विरक्ति
- प्रकृति का मनोहर स्थल काठिन्य की प्रतिमूर्ति
- अलंकारों का प्रयोग
- कविता का सहज रस बौद्धिकता से धूमिल
- उपमानों की झड़ी
- अप्रस्तुत की योजना से काठिन्य।
1. क्लिष्ट कल्पनायुक्त वर्णन- केशव की क्लिष्टता की समानता लोग जॉन मिल्टन से किया करते हैं। बडथ्वाल जी का मत है कि मिल्टन से उनकी इतनी और समानता है कि उन्होंने भी प्रकृति का परिचय काव्य परम्परा में पाया जाता है। प्रकृति के दर्शन के उपरान्त एक प्रकृति कवि की भाँति उनका हृदय आनंदित नहीं होता है। प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर उनका हृदय द्रवित नहीं होता है। उनके हृदय का विस्तार नहीं है जो प्रकृति में भी मनुष्य के सुख-दुख के लिए सहानुभूति ढूँढ़ सकता है। बेर उन्हें भयानक प्रतीत होती है, वर्षा काली का स्वरूप उपस्थित करती है और उदीयमान अरुणाय सूर्य कालातिक भरे खप्पर का स्वरूप उपस्थित करता है-
“अरुण गात अतिप्रात पद्मिनी-प्राननाथ मय।
मानहु केशवदा कोकनद कोक प्रेममय।”
2. स्वाभाविक विरह वेदना से विरक्ति- केशवदास द्वारा वर्णित राम के विरह वर्णन के प्रसंग का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि वह कोरे चमत्कार का नमूना है और केशव को कठिन काव्य का प्रेत करने के लिए बाध्य करता है।
“दीरघ दरीन बसे केसोदास केसरी ज्यो,
केसरी को देखि बनखरी ज्यों कंपत है।
बासर की संपत्ति उलूक ज्यों न चितवत,
चकवा ज्यों चंद चिते चौगुनी चम्पत है।”
उपर्युक्त प्रसंग में इतनी मार्मिकता भरी है कि किन्तु केशवदास ने अपनी पांडित्य प्रदर्शन के चक्कर में पड़कर उसे कठोरता का जामा पहना दिया।
3. प्रकृति का मनोहर स्थल काठिन्य की प्रतिमूर्ति- पंचवटी के रमणीय वातावरण का चित्रण करते समय केशव की चमत्कारप्रियता के प्रति मोह तो लक्षित होता है, परंतु उसमें प्रकृति के मनोरम रूप की झांकी नहीं मिलती।
केशवदास जी ने अपने काव्यगत रचनाओं में प्रकृति का चित्रण प्रायः किया है। इनकी रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ सुंदर चित्रण किया है। वे चाहते तो प्रकृति का स्वच्छद व स्वाभाविक चित्रण कर प्रकृति कवि के रूप में प्रसिद्ध हो सकते थे। परन्तु वैभव और विलासिता के बीच रहकर उनकी मनोवृत्ति कलापक्ष की ओर ज्यादा ही रही। इन्होंने संस्कृत के साहित्य को अधिक महत्त्व दिया था। इसलिए उन्होंने अपने काव्य को सुंदर बनाने के लिए हृदय की अपेक्षा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज्यादा किया। केशवदास जी ने एक कवि नहीं बल्कि एक सम्प्रदाय की दृष्टि से अपने काव्य को एक विशेष स्थान दिलाकर साहित्य में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाया।
4. अलंकारों का प्रयोग- केशवदास अलंकार सम्प्रदायवादी आचार्य कवि थे। इसलिए स्वाभाविक था कि वे भामह, उद्भट और दंडी आदि अलंकार सम्प्रदाय के आचार्यों का अनुसरण करते। इन्होंने अलंकारों के दो भेद माने हैं, साधारण और विशिष्ट। साधारण के अंतर्गत वर्णन, वर्णय, मूमिश्री वर्णन और राज्यश्री वर्णन आते हैं जो काव्य कल्पनावृत्ति और अलंकार-शेखर पर आधारित है। इस तरह वे अलंकाय और अलंकार में भेद नहीं मानते। अलंकारों के प्रति विशिष्ट (विशेष) रुचि होने के कारण काव्यपक्ष दब गया और सामान्यतः ये सहृदय कवि नहीं माने जाते। अपनी क्लिष्टता के कारण ये कठिन काव्य के प्रेत कहे गऐ हैं। अलंकार का उदाहरण निम्नलिखित है-
“सुंदर सुवास अरु कोमल अमल अति,
सीता जू को मुख सखि केवल कमल सो।।”
इसमें प्रायः उपमा अलंकार है।
5. उपमानों की झड़ी- केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने के पीछे एक कारण यह भी है कि उन्होंने अपने काव्य में अमानों की झड़ी लगा दी है। अशोक वाटिका में सीता जी के बैठने का एक दृश्य अवलोक्य है-
“ग्रसी बुद्धि सी चित्त चिंतामणि मानों।
किधो जीव दन्तावली में बखानों।
किधौ घोरी के राहु नारी न लीनी।
कलाचन्द्र की चारू पीयूष भीनी।”
6. अप्रस्तुत की योजना से काठिन्य- केशव के काव्य में अप्रस्तुतों की योजना के कारण भी क्लिष्टता के दर्शन होते हैं। रावण के हाथों में पड़ी हुई तथा निरीहावस्था में अशोक वाटिका में वन्दिनी सीता के हेतु केशव ने अप्रस्तुतों की जो योजना की है उसमें पर्याप्त दुरूहता उपस्थित हो गयी है-
“धूमपुर के निकेत मानो धूमकेतु की
शिखा के धूमयोनी मध्य रेखा सुखधाम की8।
चित्रका सी पुत्रिका के रूरे बगरूर माहि,
शम्बर छडाई लई कामिनी कै काम की।”
उपयुक्त पंक्ति में तो इस प्रकार की हृदयहीनता लक्षित होती है कि इसे काव्य की परिधि से निकालने की बात भी सोची जाऐ तो अनुचित नहीं होगा। केशवदास के काव्य में सहज आनंद के स्थान पर बुद्धि कसरत हुई प्रतीत होती है। पांडित्य, प्रदर्शन, अतिशय बौद्धिकता तथा छंदों का अजायबघर तैयार करने के लोभ से भी उनकी कवित्व शक्ति का ठीक-ठीक अंतर्भाव नहीं हो सकता। परिणाम स्वरूप उनका काव्य दुरूह एवं क्लिष्ट हो गया है। ‘रामचन्द्रिका’ केशवदास द्वारा लिखित परम्परा का महाकाव्य है।
स्पष्ट है कि केशवदास की सम्पूर्ण रामचंद्रिका एक दुर्बोध चमत्कारी काव्य है। केशव में सरसता, सरलता एवं स्वाभाविकता उतनी नहीं, जितनी की चमत्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति है। यही कारण है कि केशवदास हिंदी काव्य जगत में कठिन काव्य के प्रेत के नाम से विख्यात है।
